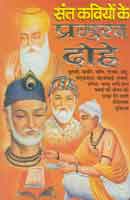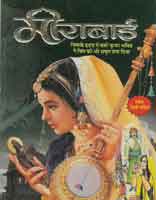|
राजनैतिक >> रेत की कगार रेत की कगारमहेन्द्र मित्तल
|
309 पाठक हैं |
|||||||
एक सामाजकि उपन्यास....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस देश की संस्कृति के रक्षक ‘पाप’ और पुण्य की भूलभुलैया को
धर्मभीरू लोगों के जीवन में सदैव से ही उतारते चले आये हैं। पाप का नाश
करना ही उनके जीवन का आदर्श है। लेकिन आज के युग में यह आदर्श कितना खोखला है और आदमी अपने पल-पल जन्म लेने वाले स्वार्थ के वशीभूत होकर, किस तरह अपने लोगों को रेत की कगार पर ले जाकर खड़ा कर देता है, यह इस उपन्यास का प्रतिपाद्म विषय है।
गाँधी जी ने सत्य की खोज में अपना समस्त जीवन होम कर दिया था। परन्तु आज का राजनीतिज्ञ, ‘सत्य’ के नाम पर असत्य के इतने बीज इस धरती में डालता चलता है, कि भविष्य में उन बीजों के अंकुर कैसे फूटेंगे, उसकी कल्पना पहले से ही की जा सकती है।
महाविद्यालयी संस्कृति के भीतर पनपने वाला यह स्वार्थी तन्त्र ‘रेत की कगार’ में जीवन्त हो उठा है।
गाँधी जी ने सत्य की खोज में अपना समस्त जीवन होम कर दिया था। परन्तु आज का राजनीतिज्ञ, ‘सत्य’ के नाम पर असत्य के इतने बीज इस धरती में डालता चलता है, कि भविष्य में उन बीजों के अंकुर कैसे फूटेंगे, उसकी कल्पना पहले से ही की जा सकती है।
महाविद्यालयी संस्कृति के भीतर पनपने वाला यह स्वार्थी तन्त्र ‘रेत की कगार’ में जीवन्त हो उठा है।
एक
पसीने से लथपथ वह घर लौटा था। तभी दोनों बच्चों ने उस पकड़ लिया और पूछने
लगे-‘‘पापा ! क्या लाये दिल्ली से ? हमारे लिए क्या लाये हो बोलो ?’’
उसकी सांसें उमस भरी गर्मी के कारण ठिकाने नहीं थी। थोड़ा सिर में दर्द भी हो रहा था। हाथ में पकड़ी हुई थीसिस का भारी बोझा उसके हाथों को तोड़े डाल रहा था। थीसिस के झोले को चारपाई पर पटक कर, टाई की नाट ढीली करते हुए वह झुंझलाया परे हटो कम्बख्तों। जरा सांस तो लेने दो।’’
बच्चे डांट खाकर थोड़ा सहम गये थे। उसने अपनी पतलून से कमीज का पल्ला बाहर खींचा और उसे पंखे की तरह ऊपर-नीचे झुलाता हुआ अपने आपको हवा करने लगा। हवा बिलकुल बन्द थी और चिपचिपाती हुई उमस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। कमीज के पल्ले से ही पसीने से भीगा अपना मुंह अपने पोंछा और गर्दन पर उभर आये पानी को रगड़ता हुआ जरा ऊँची आवाज में चिल्लाया-अरे भई कहां हो ? एक गिलास पानी मिलेगा क्या इस घर में ?’’
‘आई जी !’’ तुरन्त ही बरामदे के दूसरे छोर पर बनी हुई रसोई से मानो जबरदस्ती तेज किया हुआ एक स्वर वहां तक पहुंचा था।
बच्चे अभी तक सहमे हुए उसके सामने खड़े थे। वे कभी अपने पापा की ओर देख लेते थे, तो कभी चारपाई पर पड़े उस भारी भरकम थैले की ओर। उन्हें जैसे आशा थी कि पापा उसमें उनके लिए कुछ न कुछ जरूर लाये होंगे।
हाथ में पानी का गिलास लिए, तभी एक दुबली-पतली स्त्री उसके सामने आ खड़ी हुई थी और पानी का गिलास हाथों में पकड़ा कर बच्चों से बोली थी-‘‘तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में आते ही मत चिपटा करो। लेकिन तुम हो कि एक बार चिमगादड़ की तरह चिपट कर पीछा ही नहीं छोड़ते।’’
‘‘रहने दो उमा।’’ पानी का गिलास एक ही सांस में खाली करके वह बोला-‘‘इनसे कहो कि मैं आज कुछ नहीं ला सका। इन्टरव्यू के बाद वहां से सीधा यहीं चला आ रहा हूं।’’ फिर बच्चों को चुपचाप खड़े देखकर वह स्वयं ही उनसे बोला था-‘‘जाओ बेटो खेलो जाकर। इस बार मैं जब भी दिल्ली जाऊंगा, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजें लेकर आऊंगा।’’
बच्चे मायूस होकर वहां से चले गये थे। उमा पंखे का स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ी-‘‘पंखा ही खोल लिया होता।’’ लेकिन स्विच ऑन करने पर भी जब बिजली का पंखा नहीं चला तो वह झुंझलाई, सत्यनाश हो इन बिजली वालों का। इतनी गर्मी पड़ रही है और ये लोग हैं कि आराम से बिजली बन्द किये बैठे हैं।’’ पास पड़ा हाथ का पंखा उठा कर उसने पूछा-‘‘क्या रहा ? कुछ काम बना?’’
‘‘बिना अप्रोच के आजकल कहीं काम बनता है?’’ उत्तर में उलटे उसी ने उमा से प्रश्न कर दिया था।
पल भर उमा चुप रही थी। फिर बोली-‘‘तुम तो बेकार में दिल्ली के पीछे पड़े हो। यहां तुम्हें किस बात की कमी है ? अच्छा कालेज है, अच्छी नौकरी है।’’
‘‘हां, अच्छी नौकरी है, अच्छा कालेज है।’’ एक फीकी मुस्कान उसके ओठों पर तैर आयी। वह उठा और एक गहरी सांस छोड़कर कपड़े बदलने लगा।
संध्या आयी थी, पर रात होने में अभी देर थी। थोड़ा सुस्ताने के लिए वह चारपाई पर लेट गया। उमा पंखा उसके पास छोड़ कर रसोई की ओर चली गयी थी।
उसके शब्द कुछ पलों तक वहां तैरते रहे थे। ‘‘अच्छा कालेज है, अच्छी नौकरी है।’’
परिस्थितियां बदल गयी थीं। स्थान बदल गया था। समय-समय पर सम्पर्क सूत्रों में बंधने वाले न जाने कितने नये-नये चेहरे, सामने आकर बिखर गये थे। पर उसे लग रहा था कि जिस कड़वी घूंट को निगलने के डर से घबरा कर, वह अपने पहले, दूसरे और तीसरे स्थानों को छोड़कर भाग आया था, वही घूंट अब पुनः उसके हलक के नीचे उतर जाने के लिए मुंह में घुलती जा रही थी। पर वह नीलकंठ नहीं बन सका था। वह कोई तपस्वी भी नहीं था। उसे लग रहा था कि सृष्टि का जैसे कोई कल्पित देवता, आधुनिक डाक्टर का रूप धरे उसकी छाती पर आकर खड़ा हो गया था। और उससे बार-बार कह रहा था।–‘‘इसे पिओ। इसे पिओ रमाकान्त। तुम्हें इसे पीना ही होगा। जब तक यह घूंट तुम अपने हलक से नीचे नहीं उतार लोगे तब तक मैं तुम्हारी छाती पर से नहीं हटूंगा।’’
उसका दम घुटने लगा था। भयानक दर्द से उसकी छाती फटने लगी थी। बेचैनी से धौंकनी बना उसका सीना हफ्-हफ् करने लगा था। बड़ी मुश्किल से वह भाग निकलने में सफल हुआ था। एक बार भागा तो फिर भागना है, भागते रहना है। उसे तब तक भागते रहना है, जब तक उसकी सांसें पूरी तरह से उखड़ नहीं जातीं और वह बेदम होकर गिर नहीं पड़ता।
उसे लगा था कि जिस दायरे में वह अब तक खड़ा था वह बहुत छोटा था। उसे किसी बड़े दायरे की जरूरत थी। अपनी इसी जररूत के लिए उसने दायरे को फैलाना चाहा था। पर वह टूट गया था। बहुत अधिक हवा भरते चले जाने पर जैसे कोई गुब्बारा फट पड़ता है, उसी तरह वह भी फट पड़ा था। उसे लग रहा था कि बरसों से जिस लक्ष्य और दिशा के लिए उसका अहम भटकता रहा था वह अभी भी उससे कोसों दूर था। उसे लगता कि हर बार उसकी जिन्दगी से बंधे तीन मासूम चेहरे उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वे उसे रोक लेते हैं और केवल एक ही दिशा की ओर चलते रहने के लिए उसे विवश करते हैं। और वह, न चाहते हुए भी उसे ओर चल पड़ता है। चलता रहता है...पिछली बार उमा ने कहा था-‘‘सुनो। इस बार सर्दियों के लिए कुछ पैसा बचाकर रख लेना, शायद जरूरत पड़ जाये।’’
तभी उसे तीन के स्थान पर चार आकारों की चिन्ता सताने लगी थी। सोचा था कि अब जल्दी ही उसे कोई सही दिशा पकड़ लेनी चाहिए। पर वह सही दिशा कौन-सी थी ? किस दशा की ओर बढ़ते हुए वह उनके अस्तित्व की रक्षा करने में सक्षम हो सकता था ? वह अभी तक नहीं समझ पाया था।
ये ऐसे प्रश्न थे, जो प्रश्न ही रह गये थे। तब भी और आज भी। पन्द्रह अगस्त को भारत ने अपनी स्वन्तत्रता की एक बार फिर से साल गिरह मनाई थी। एक बार फिर, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर तिंरगा झंड़ा लहराया गया था। पर उसने अपनी जिन्दगी के बत्तीसवें अगस्त में फिर से पराधीनता स्वीकार कर ली थी। शायद यही उसकी नियति थी।
उसकी सांसें उमस भरी गर्मी के कारण ठिकाने नहीं थी। थोड़ा सिर में दर्द भी हो रहा था। हाथ में पकड़ी हुई थीसिस का भारी बोझा उसके हाथों को तोड़े डाल रहा था। थीसिस के झोले को चारपाई पर पटक कर, टाई की नाट ढीली करते हुए वह झुंझलाया परे हटो कम्बख्तों। जरा सांस तो लेने दो।’’
बच्चे डांट खाकर थोड़ा सहम गये थे। उसने अपनी पतलून से कमीज का पल्ला बाहर खींचा और उसे पंखे की तरह ऊपर-नीचे झुलाता हुआ अपने आपको हवा करने लगा। हवा बिलकुल बन्द थी और चिपचिपाती हुई उमस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। कमीज के पल्ले से ही पसीने से भीगा अपना मुंह अपने पोंछा और गर्दन पर उभर आये पानी को रगड़ता हुआ जरा ऊँची आवाज में चिल्लाया-अरे भई कहां हो ? एक गिलास पानी मिलेगा क्या इस घर में ?’’
‘आई जी !’’ तुरन्त ही बरामदे के दूसरे छोर पर बनी हुई रसोई से मानो जबरदस्ती तेज किया हुआ एक स्वर वहां तक पहुंचा था।
बच्चे अभी तक सहमे हुए उसके सामने खड़े थे। वे कभी अपने पापा की ओर देख लेते थे, तो कभी चारपाई पर पड़े उस भारी भरकम थैले की ओर। उन्हें जैसे आशा थी कि पापा उसमें उनके लिए कुछ न कुछ जरूर लाये होंगे।
हाथ में पानी का गिलास लिए, तभी एक दुबली-पतली स्त्री उसके सामने आ खड़ी हुई थी और पानी का गिलास हाथों में पकड़ा कर बच्चों से बोली थी-‘‘तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में आते ही मत चिपटा करो। लेकिन तुम हो कि एक बार चिमगादड़ की तरह चिपट कर पीछा ही नहीं छोड़ते।’’
‘‘रहने दो उमा।’’ पानी का गिलास एक ही सांस में खाली करके वह बोला-‘‘इनसे कहो कि मैं आज कुछ नहीं ला सका। इन्टरव्यू के बाद वहां से सीधा यहीं चला आ रहा हूं।’’ फिर बच्चों को चुपचाप खड़े देखकर वह स्वयं ही उनसे बोला था-‘‘जाओ बेटो खेलो जाकर। इस बार मैं जब भी दिल्ली जाऊंगा, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीजें लेकर आऊंगा।’’
बच्चे मायूस होकर वहां से चले गये थे। उमा पंखे का स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ी-‘‘पंखा ही खोल लिया होता।’’ लेकिन स्विच ऑन करने पर भी जब बिजली का पंखा नहीं चला तो वह झुंझलाई, सत्यनाश हो इन बिजली वालों का। इतनी गर्मी पड़ रही है और ये लोग हैं कि आराम से बिजली बन्द किये बैठे हैं।’’ पास पड़ा हाथ का पंखा उठा कर उसने पूछा-‘‘क्या रहा ? कुछ काम बना?’’
‘‘बिना अप्रोच के आजकल कहीं काम बनता है?’’ उत्तर में उलटे उसी ने उमा से प्रश्न कर दिया था।
पल भर उमा चुप रही थी। फिर बोली-‘‘तुम तो बेकार में दिल्ली के पीछे पड़े हो। यहां तुम्हें किस बात की कमी है ? अच्छा कालेज है, अच्छी नौकरी है।’’
‘‘हां, अच्छी नौकरी है, अच्छा कालेज है।’’ एक फीकी मुस्कान उसके ओठों पर तैर आयी। वह उठा और एक गहरी सांस छोड़कर कपड़े बदलने लगा।
संध्या आयी थी, पर रात होने में अभी देर थी। थोड़ा सुस्ताने के लिए वह चारपाई पर लेट गया। उमा पंखा उसके पास छोड़ कर रसोई की ओर चली गयी थी।
उसके शब्द कुछ पलों तक वहां तैरते रहे थे। ‘‘अच्छा कालेज है, अच्छी नौकरी है।’’
परिस्थितियां बदल गयी थीं। स्थान बदल गया था। समय-समय पर सम्पर्क सूत्रों में बंधने वाले न जाने कितने नये-नये चेहरे, सामने आकर बिखर गये थे। पर उसे लग रहा था कि जिस कड़वी घूंट को निगलने के डर से घबरा कर, वह अपने पहले, दूसरे और तीसरे स्थानों को छोड़कर भाग आया था, वही घूंट अब पुनः उसके हलक के नीचे उतर जाने के लिए मुंह में घुलती जा रही थी। पर वह नीलकंठ नहीं बन सका था। वह कोई तपस्वी भी नहीं था। उसे लग रहा था कि सृष्टि का जैसे कोई कल्पित देवता, आधुनिक डाक्टर का रूप धरे उसकी छाती पर आकर खड़ा हो गया था। और उससे बार-बार कह रहा था।–‘‘इसे पिओ। इसे पिओ रमाकान्त। तुम्हें इसे पीना ही होगा। जब तक यह घूंट तुम अपने हलक से नीचे नहीं उतार लोगे तब तक मैं तुम्हारी छाती पर से नहीं हटूंगा।’’
उसका दम घुटने लगा था। भयानक दर्द से उसकी छाती फटने लगी थी। बेचैनी से धौंकनी बना उसका सीना हफ्-हफ् करने लगा था। बड़ी मुश्किल से वह भाग निकलने में सफल हुआ था। एक बार भागा तो फिर भागना है, भागते रहना है। उसे तब तक भागते रहना है, जब तक उसकी सांसें पूरी तरह से उखड़ नहीं जातीं और वह बेदम होकर गिर नहीं पड़ता।
उसे लगा था कि जिस दायरे में वह अब तक खड़ा था वह बहुत छोटा था। उसे किसी बड़े दायरे की जरूरत थी। अपनी इसी जररूत के लिए उसने दायरे को फैलाना चाहा था। पर वह टूट गया था। बहुत अधिक हवा भरते चले जाने पर जैसे कोई गुब्बारा फट पड़ता है, उसी तरह वह भी फट पड़ा था। उसे लग रहा था कि बरसों से जिस लक्ष्य और दिशा के लिए उसका अहम भटकता रहा था वह अभी भी उससे कोसों दूर था। उसे लगता कि हर बार उसकी जिन्दगी से बंधे तीन मासूम चेहरे उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वे उसे रोक लेते हैं और केवल एक ही दिशा की ओर चलते रहने के लिए उसे विवश करते हैं। और वह, न चाहते हुए भी उसे ओर चल पड़ता है। चलता रहता है...पिछली बार उमा ने कहा था-‘‘सुनो। इस बार सर्दियों के लिए कुछ पैसा बचाकर रख लेना, शायद जरूरत पड़ जाये।’’
तभी उसे तीन के स्थान पर चार आकारों की चिन्ता सताने लगी थी। सोचा था कि अब जल्दी ही उसे कोई सही दिशा पकड़ लेनी चाहिए। पर वह सही दिशा कौन-सी थी ? किस दशा की ओर बढ़ते हुए वह उनके अस्तित्व की रक्षा करने में सक्षम हो सकता था ? वह अभी तक नहीं समझ पाया था।
ये ऐसे प्रश्न थे, जो प्रश्न ही रह गये थे। तब भी और आज भी। पन्द्रह अगस्त को भारत ने अपनी स्वन्तत्रता की एक बार फिर से साल गिरह मनाई थी। एक बार फिर, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर तिंरगा झंड़ा लहराया गया था। पर उसने अपनी जिन्दगी के बत्तीसवें अगस्त में फिर से पराधीनता स्वीकार कर ली थी। शायद यही उसकी नियति थी।
दो
साहिबाबाद का ‘गांधी महाविद्यालय’ पिछले सात वर्ष से
ही
अस्तित्व में आया था। नींव रखने वाले थे प्रदेश के मुख्यमंत्री। उस समय
इसे कुछ अस्सी छात्रों और तीन अध्यापकों के सहयोग से प्रारम्भ किया गया
था। आज छात्र-छात्राओं की संख्या आठ सौ थी और प्राध्यापक सत्रह थे। वह
सबसे बाद में आने वाला प्राध्यापक था। अट्ठारहवां।
उसने जिस दिन इस महाविद्यालय के शिक्षाविदों के मध्य अपने को पहली बार घिरा हुआ पाया था उसी दिन उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ था कि दुर्भाग्य से वह ऐसे लोगों के बीच फिर से आ फंसा है, जिन्हें वह सदैव से नापसन्द करता आया था। उसे लगा कि वह कहीं भी भागकर चला जाये, उनसे पीछा छुड़ा लेना इतना आसान नहीं था जितना वह समझता था।
‘स्टाफ रूम’ में प्रवेश करने पर कितनी ही जिज्ञासु आंखें उसके हर परिचय को एक ही पल में जान लेना चाहती थीं। पल भर के लिए अपरिचित व्यक्तित्व की सीमाओं में वह लज्जा से सिमट गया था। किन्तु दूसरे ही क्षण उन्हें संबोधित करते हुए वह बोला था-‘नमस्कार मित्रों। मेरा नाम रमाकान्त है और मैं यहां हिन्दी विभाग में...।’’
‘‘आओ आओ !’’ बीच में ही उसकी बात काट कर एक ठिगने कद का पहाड़ी युवक बड़ी गर्मजोशी के साथ उठ कर आगे बढ़ा था-‘‘नमस्कार। हमें मालूम है, आपकी यहां पोस्टिंग हुई है। आइये बैठिये। हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।’’ और उसने कस कर उसका हाथ दबा दिया था।
बारी-बारी से वहां बैठे अन्य तीन व्यक्तियों से भी शिष्टाचार वश उसे हाथ मिलाना पड़ा था। उसे लगा था कि कुछ ही देर में उन्होंने उसकी सारी परतें उखाड़ फेंकी हैं। वह कहां का रहने वाला है, शादीशुदा है या क्वांरा है, कब उसने एम.ए. किया, कहां से किया, किस डिवीजन में पास किया, अब तक क्या करता रहा, इन्टरव्यू में क्या-क्या पूछा गया, कुछ शर्ते भी लगाई थीं या नहीं, यहां पर कहां और कब तक रहने का इरादा है....आदि आदि।
इस प्रकार महाविद्यालय में प्रवेश करने का एक और इन्टरव्यू देकर वह चुप होने जा रहा था कि उनमें से एक प्रोफेसर महोदय ने जो शायद अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे थे, इस बीच दो कप चाय मंगा ली थी। एक उसके लिए और इस सम्भवतः अपने लिए।
उसने जिस दिन इस महाविद्यालय के शिक्षाविदों के मध्य अपने को पहली बार घिरा हुआ पाया था उसी दिन उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ था कि दुर्भाग्य से वह ऐसे लोगों के बीच फिर से आ फंसा है, जिन्हें वह सदैव से नापसन्द करता आया था। उसे लगा कि वह कहीं भी भागकर चला जाये, उनसे पीछा छुड़ा लेना इतना आसान नहीं था जितना वह समझता था।
‘स्टाफ रूम’ में प्रवेश करने पर कितनी ही जिज्ञासु आंखें उसके हर परिचय को एक ही पल में जान लेना चाहती थीं। पल भर के लिए अपरिचित व्यक्तित्व की सीमाओं में वह लज्जा से सिमट गया था। किन्तु दूसरे ही क्षण उन्हें संबोधित करते हुए वह बोला था-‘नमस्कार मित्रों। मेरा नाम रमाकान्त है और मैं यहां हिन्दी विभाग में...।’’
‘‘आओ आओ !’’ बीच में ही उसकी बात काट कर एक ठिगने कद का पहाड़ी युवक बड़ी गर्मजोशी के साथ उठ कर आगे बढ़ा था-‘‘नमस्कार। हमें मालूम है, आपकी यहां पोस्टिंग हुई है। आइये बैठिये। हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।’’ और उसने कस कर उसका हाथ दबा दिया था।
बारी-बारी से वहां बैठे अन्य तीन व्यक्तियों से भी शिष्टाचार वश उसे हाथ मिलाना पड़ा था। उसे लगा था कि कुछ ही देर में उन्होंने उसकी सारी परतें उखाड़ फेंकी हैं। वह कहां का रहने वाला है, शादीशुदा है या क्वांरा है, कब उसने एम.ए. किया, कहां से किया, किस डिवीजन में पास किया, अब तक क्या करता रहा, इन्टरव्यू में क्या-क्या पूछा गया, कुछ शर्ते भी लगाई थीं या नहीं, यहां पर कहां और कब तक रहने का इरादा है....आदि आदि।
इस प्रकार महाविद्यालय में प्रवेश करने का एक और इन्टरव्यू देकर वह चुप होने जा रहा था कि उनमें से एक प्रोफेसर महोदय ने जो शायद अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे थे, इस बीच दो कप चाय मंगा ली थी। एक उसके लिए और इस सम्भवतः अपने लिए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i